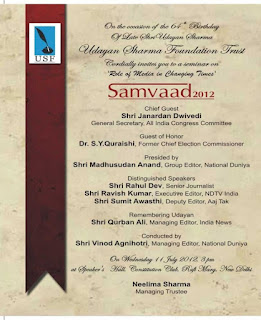अन्ना सीजन वन और सीजन टू में टाटा से लेकर महिन्द्रा कंपनी ने अन्ना का समर्थन करके सरकार को आगाह कर दिया था कि अगर संसद के भीतर की चीजें हमारे मुताबिक नहीं हुई तो हम संसद के बाहर का मौहाल इतनी गर्म कर देंगे कि संसद के भीतर के लोग अपने आप महत्वहीन हो जाएंगे. टाटा डोकोमो ने ब्रांड अन्ना ऑफर और कॉलर ट्यून जारी किए, रतन टाटा ने देश के उद्योगपतियों से इस आंदोलन में साथ आने की अपील की. बजाज हमेशा साथ खड़े होने की बात की. ये वो सारी कार्पोरेट कंपनियां हैं जो तथाकथित भ्रष्ट सरकार के अपने साथ न दिए जाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो गई थी.
चूंकि मीडिया और कार्पोरेट ममेरे-फुफेरे भाई हैं तो मीडिया ने भी जमकर इस अन्ना सीजन 1 और 2 का साथ दिया. न्यूजरुम के सारे सूरमा शीतप्रभाव(एसी) से निकल जंतर-मंतर पर जमा हुए. कटिंग चाय और कीन्ले की दम पर घंटों पीटूसी देते-करते रहे..चैनल के मालिकों के लिए ये भले ही मिले सुर मेरा तुम्हारा था लेकिन कुछ मीडियाकर्मियों के लिए जंतर-मंतर और रामलीला मैंदान कॉन्फेशन सेंटर थे जहां वे अपनी गर्दन की नसें फुलाकर पहले के कर्मों की प्रायश्चित इस सीजन के पक्ष में बात करके कर रहे थे. एक ही साथ कई सुरमाओं ने आवाज लगायी जिसमें सबसे उंचा स्वर अर्णव गोस्वामी का था. वो इसलिए भी कि उनकी मदर कंपनी की साख राष्ट्रमंडल खेल की ठेकेदारी न मिलने और पेड न्यूज प्रस्ताव की बात कैग की रिपोर्ट में सामने आने के बाद बुरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी और उन्हें ये दाग धोने थे. इस उंचे स्वर में अपने आइबीएन7 के आशुतोष का स्वर इतना गहरा गया कि जॉन रीड की "दस दिन दुनिया जब हिल उठी" की तर्ज पर अन्ना आंदोलन के पक्ष में पूरी की पूरी एक किताब ही लिख डाली और अगर उस दौरान की बहसों की फुटेज देखें तो आशुतोष आपको अन्ना कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आएंगे. आशुतोष को अगर अपनी सैलरी की चिंता नहीं व्यापती तो जिस तरह जे पी आंदोलन में कई पेशेवर पत्रकार शामिल हुए थे, सब छोड़-छाड़कर वो भी इस सीजन में कूदते. लेकिन
अब यही चैनल आइबीएन7 भरी-पूरी भीड़ दिखाते हुए भी कह रहा है कि मैंदान खाली है. लोग नहीं जुट रहे हैं. आम आदमी नजर नहीं आ रहा. सवाल ये नहीं है कि लोग जुट रहे हैं कि नहीं. सवाल है कि क्या अब तक मीडिया जिस भ्रष्टाचार की मुहिम का साथ दे रहा था( हालांकि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल का हिस्सा था), अब सब दुरुस्त हो गया. हमें तो लगा था कि कोई नहीं तो कम से कम नेटवर्क18 ग्रुप के चैनल सरकार के विरोध में खड़े होंगे क्योंकि उस पर सीधे अंबानी का हाथ है लेकिन नहीं. उसकी वेबसाइट ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि अन्ना आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है..तो जनाब ये होती है सत्ता के पक्ष की जुबान. भूतपर्व स्टार न्यूज जो अब एबीपी न्यूज है ने सुपर लगाया- अन्ना का फ्लॉप शो ? जिस मीडिया और चैनल के लिए पिछले साल अन्ना का रियलिटी शो आंदोलन था और जब ये बात हम-आप कहते थे लोग कोडे बरसाने की मुद्रा में आ जाते थे. आज एक चैनल इस आंदोलन को शो बता रहा है तो कोई उससे सवाल करनेवाला नहीं है कि जिस आंदोलन में हजारों लोग शामिल हैं, उसे आप शो कैसे कह सकते हैं और सारी बहस परफॉर्मेंस पर क्यों हो रही है, मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही ? क्या लोगों के कम जुटने से सारे मुद्दे खत्म हो गए और फिर जो बेशर्म मीडिया बार-बार सवाल कर रहा है कि लोग कहां गए, कोई उनसे भी तो पूछे कि लोगों का तो छोड़िए, आप कहां गए ? कल तक तो आप टीम अन्ना के चीयरलीडर और कार्यकर्ता बने फिरते थे.
अब कोई अर्णव से जाकर पूछे कि मीडिया इज अन्ना और अन्ना इज मीडिया का नारा कहां गया. वी सपोर्ट अन्ना के सुपर कहां गए और द टाइम्स ऑफ इंडिया का इश्तहार. भाईजी, हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मीडिया शरीर का बुखार तक मुफ्त में नहीं देता,कवरेज कहां से देगा ? अब देखिएगा केजरीवाल और उनके वृंदों की जुबान उस मीडिया के खिलाफ जल्द ही खुलेगी जिसे अब तक मसीहा मानकर थै-थै कर रहे थे. चैनलों के एक-एक स्लग,सुपर,पीटूसी और एंकर लाइन अन्ना सीजन4 को कमजोर करने में जुटे हैं और इस हालत तक ला छोड़ेगे कि विजयादशमी तक केजरीवाल के पुतले फूंके जाएंगे और क्या पता अबकी बार सोनियाजी लाल किला जाकर रावण के पुतले में नहीं, उनके ही पुतले में बत्ती लगा आए.