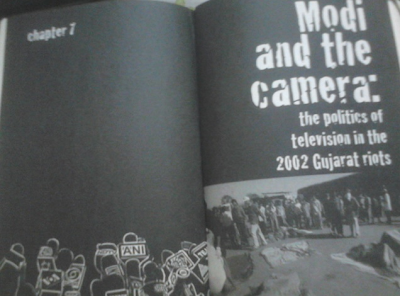इन दिनों टेलीविजन संसद में थाली विमर्श जोरों पर है. ऐसे जैसे कभी पूरी राजनीति राम जन्मभूमि मंदिर-मस्जिद विवाद की तरफ लप्प( झुकना) जाती है तो कभी मोदी बयान पर कल्टी खाने लगती है. इस थाली की सियासत की अपनी कहानी है जो हमारे ट्विट और एफबी स्टेटस की तरह जल्द ही गुम हो जाएंगे..लेकिन इस थाली शब्द के दिन-रात कान में गूंजते रहने के बीच क्या हम पांच रुपये या 12 रुपये की थाली की कल्पना से खिसककर एक ऐसी थाली की कल्पना के बजाय सीधे किचन में बनाने घुस सकते हैं, जिनकी दोस्ती-यारी,प्यार-मोहब्बत में खिलाने पर कोई कीमत न हो और अगर दिन-दशा खराब होने लगे तो जीने लायक पैसे मिल जाएंगे. इसी तुक्का-फजीहत में अपने तैयार की शनिवारी थाली. हमारे रेगुलर पाठकों के लिए भारी-भरकम विमर्श के बीच ये निहायत ही बकवास पोस्ट लगे लेकिन क्या पता इनसे कुछ जो आए दिन संतनगर,बुराड़ी,पांडवनगर में अकेले हडिया हिलाते-डुलाते रहते हैं, उन्हें इस शहर में यारबाजी का एक विकल्प मिल जाए, बस इसी नीयत से-
शनिवारी थालीः बैचलर्स किचन की खास पेशकश

खाद्य सामग्रीः कढ़ी, भात( चावल नहीं), आलू भुजिया, पापड़, खीरे की सलाद
शनिवारी थालीः बैचलर्स किचन की खास पेशकश